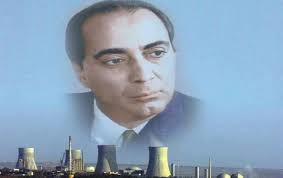जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर (Julius Robert Oppenheimer) (२२ अप्रैल १९०४ - १८ फ़रवरी १९६७) एक सैद्धान्तिक भौतिकविद् एवं अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (बर्कली) में भौतिकी के प्राध्यापक थे। लेकिन वे परमाण बम के जनक के रूप में अधिक विख्यात हैं। वे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिये आरम्भ की गयी मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक थे। न्यू मैक्सिको में जब ट्रिनिटी टेस्ट हा और इनकी टीम ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उनके मुंह से भगवद गीता का एक श्लोक निकल पड़ा।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।
यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः॥१२॥
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।...॥३२॥
मैनहट्टन परियोजना
सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा परमाणु उर्जा की थ्योरी विकसित करने का श्रेय आइंस्टाइन को जाता है जिसके आधार पर तकरीबन चालीस साल बाद परमाणु बम बनाया गया। १९३८ तक यह थ्योरी थ्योरी ही रही। उस साल तीन जर्मन वैज्ञानिकों ने एक खोज की। ओट्टो हान, लीजे माइत्नेर और फ्रित्ज़ स्ट्रास्मान ने पाया कि यदि यूरेनियम पर न्युट्रान बरसाया जाए तो उससे बेरियम और क्रिप्टन उत्सर्जित होते हैं और इस प्रक्रिया से बहुत गर्मी पैदा होती है जिसे न्यूक्लिअर फ़िज़न कहते हैं। तकरीबन इसी वक़्त डेनिश मूळ के वैज्ञानिक नील्स हेनरिक डेविड बोअर ने महसूस किया कि इस प्रकिया के द्वारा सामरिक हथियार विकसित किया जा सकता है। अगले साल १९३९ में नील्स अमेरिका चले गए। उनका उद्देश्य अमेरिका को इस तरह के हथियार पर काम करने के लिए चेताना था और वे चाहते थे अमेरिका इसपर जर्मनी से पहले सफलता प्राप्त करे। जिस ओर जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में जा रहा था यह कदम ज़रूरी भी लग रहा था।
नील्स ने अमेरिका पहुँच कर हंगेरियन मूल के भौतिकशास्त्री लियो स्जिलार्ड से संपर्क साधा और उन्हें इस बारे में बताया। लियो ने तत्काल आइंस्टाइन से बात की जोकि अमेरिका में ही थे। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने ही न्यूक्लिअर फ़िज़न के दरवाज़े खोले थे और वे विश्व के निर्विवाद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन ने राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को २ अगस्त १९३९ को वह मशहूर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिका को जर्मनी द्वारा इस ओर प्रयोग करने के बाबत लिखा और चेताया कि नाज़ियों द्वारा इस तरह का अस्त्र बनाने में सफलता पाने से विश्व भर के लिए क्या खतरा हो सकता है। हालाँकि बाद में उन्होंने अपने इस पत्र पर अफ़सोस व्यक्त किया मगर भविष्य में क्या होगा यह उस समय कहना सम्भव नहीं था।
असीमित संभावनाओं वाले इस संभावित अस्त्र के निर्माण को गोपनीय रखना आवश्यक था। राष्ट्रपति ने परमाणु बम को विकसित करने का काम अमेरिकी सेना के मैनहैटन विभाग को सौंपा जिसकी वजह से इस परम गोपनीय प्रोजेक्ट को मैनहैटन प्रोजेक्ट कहा जाता था। इस प्रोजेक्ट का सञ्चालन करने का जिम्मा मेजर जनरल लेसली ग्रोव्स को दिया गया और इसके निर्माण से चार यूरोपी प्रवासी जुड़े। इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सरकार में इसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि रूज़वेल्ट की आकस्मिक मृत्यु होने पर जब ट्रूमन राष्ट्रपति बने तो उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मगर साथ ही यह भी सच है कि कुछ लोगों ने सोवियत, जोकि उस समय अमेरिका का युद्ध में सहयोगी था, को इस प्रोजेक्ट के कुछ गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराये थे।
अब सबसे पहले एक न्यूक्लिअर रिएक्टर बनाने की आवश्यकता थी जिसके द्वारा चेन-रिअक्शन किया जा सके। यह काम शिकागो विश्वविद्यालय में इटालियन भौतिकशास्त्री एनरीको फ़ेर्मी के निर्देशन में अंजाम दिया गया। ये वही फ़ेर्मी थे जिन्हें १९३८ में न्यूटरोन फ़िज़िक्स में शोध के लिए नोबेल मिला था। शिकागो रिएक्टर में ५० टन यूरेनियम, केडमियम कंट्रोल रौड्स, ५०० टन ग्रेफाईट इस्तेमाल किया गया। चेन-रिअक्शन कराने में अगले तीन साल लगे और २ दिसम्बर, १९४२ को इसमें सफलता पायी गई। मेजर जनरल ग्रोव्स ने मैनहैटन प्रोजेक्ट के लिए गुप्त रूप से तीन केन्द्र स्थापित किए। पहला केन्द्र टेनेसी में बनाया गया जहाँ यूरेनियम-२३५ फेक्ट्री लगाई गई। इसके लिए भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत थी जो टेनेसी में नवनिर्मित हाइड्रो-इलैक्ट्रिक बांधों से उपलब्ध कराई गई। वाशिंगटन में प्लूटोनियम-२३९ केन्द्र स्थापित किया गया। तीसरा केन्द्र असल में एक प्रयोगशाला था जोकि न्यू मेक्सिको के पास लोस आलामोस में थी। यही वह जगह थी जहाँ परमाणु बम वास्तव में बनाया गया। फ़ेर्मी के साथ हंगेरियन भौतिकशास्त्री लियो स्जिलार्ड भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। ये वही लियो स्जिलार्ड थे जिन्होंने आइंस्टाइन से रूज़वेल्ट को पत्र लिखने के लिए कहा था। जिस समय फ़ेर्मी शिकागो में काम कर रहे थे लगभग उसी समय रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनके साथ कुछ और वैज्ञानिक केलिफोर्निया विश्वविद्यालय में न्यूक्लिअर फ़िज़न पर काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि यूरेनियम-२३५ के अलावा प्लूटोनियम-२३९ से भी न्यूक्लिअर फ़िज़न करना सम्भव है। इसी के आधार पर जनरल ग्रोव्स ने तीन केन्द्र स्थापित किए थे। अब रॉबर्ट ओपनहाइमर भी मैनहैटन प्रोजेक्ट से जुड़ चुके थे। चौथे वैज्ञानिक आर्थर कोम्प्टन थे जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े।
पहला परमाणु हथियार, जोकि एक यूरेनियम-२३५ बम था, का सफल प्रयोग १६ जुलाई १९४५ में न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में किया गया। इसे कोड दिया गया - ट्रिनिटी। इसके समानांतर अमेरिकी वायुसेना ने एक संगठन स्थापित किया जिसे ५०९ कोम्पोसिट ग्रुप नाम दिया गया। इस ग्रुप को अज्ञात विशाल बमों को गिराने की ट्रेनिंग दी गई और इस काम के लिए बोइंग बी-२९ बोम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। १९४५ के मध्य तक विश्व भर में सैनिक और राजनैतिक माहौल तेजी से बदल चुका था। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की अप्रैल में मृत्यु हो चुकी थी और मई में जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था। यूरोप में विश्वयुद्ध ख़त्म हो चुका था और मित्र देशों ने अपना ध्यान अबतक पूरी तरह से जापान पर केंद्रित कर लिया था। मैनहैटन प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग सभी वैज्ञानिक इसी वजह से इससे जुड़े थे ताकि जर्मनी के इस ओर सफलता हासिल करने से पहले अमेरिका या मित्र देश इसपर काम शुरू कर दें मगर जापान पर इसका इस्तेमाल हो वे इसके हिमायती नहीं थे। पर अब बात उनके चुनाव की नहीं रह गई थी। इवो जिमा और ओकिनावा में चल रहे युद्ध में मित्र देश जापान द्वारा बुरी तरह पछाडे जा चुके थे। मित्र देशों का अंदाजा था कि यदि युद्ध जापान की धरती पर इसी तरह चलता है तो लगभग दस लाख जाने जा सकती हैं और इनमे से ज्यादातर अमेरिकियों के होने की सम्भावना ट्रूमन को यह मंज़ूर नहीं था। उन्होंने अपने केबिनेट और उच्च सैनिक सलाहकारों के साथ मीटिंग के बाद तय किया कि जापान के ख़िलाफ़ दो परमाणु बमों का प्रयोग किया जाए।
पहला बम, जिसे "लिटिल बॉय" के नाम से जाना जाता है, वास्तव में लिटिल नहीं था। उसका वज़न ९,७०० पाउंड था। यह एक यूरेनियम बम था और ६ अगस्त १९४५ को इसे हिरोशिमा पर गिराया गया। इसके तीन दिन बाद अगला बम, जोकि एक प्लूटोनियम बम था, नागासाकी पर गिराया गया। इस बम का वज़न तकरीबन दस हज़ार पाउंड था. हिरोशिमा में परमाणु बम के हमले से अस्सी हज़ार लोग तो तत्काल मारे गए और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम "फैट मैन" से चालीस हज़ार लोग मारे गए। आने वाले दिनों में मरने वालों की संख्या लगभग दुगनी हो गई। जापान को लगा कि अमेरिका अगर चाहे तो ऐसे कई और परमाणु हमले जापान पर कर सकता है जोकि हालांकि सही नहीं था मगर अंततः जापान ने १५ अगस्त को मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार बनाने या प्राप्त करने में सफल न हो सके। अमेरिका को अपने प्रयासों में पहला झटका १९४९ में लगा जब अमेरिका से चोरी से प्राप्त दस्तावेज़ों के आधार पर सोवियत ने भी परमाणु बम बना लिया। इस तरह अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो गया और दुनिया प्रत्यक्ष रूप से दो धुरियों में बंट गई। इसके पीछे अमेरिका की अपना एकाधिकार बनाये रखने की कामना काम कर रही थी या उसे इस विनाशक हथियार के ग़लत इस्तेमाल की चिंता खा रही थी यह बहस का विषय हो सकता है। विश्व का अग्रणी बनकर वह कूटनीतिक और अगर ज़रूरत पड़े तो शक्ति द्वारा यह कोशिश करता आया है कि कोई भी देश परमाणु शक्ति संपन्न न बन सके किंतु ज्ञान और विज्ञान पर एकाधिकार बनाए रखने की मंशा इस युग में सम्भव नहीं है अमेरिका को यह समझना चाहिए। वैसे भी एकमात्र परमाणु हमला करने वाले देश को नैतिक स्तर पर भी यह अधिकार नहीं कि वह परमाणु शक्ति संपन्न देश का अपना स्टेटस बरकरार रखते हुए किसी और को यह साधन प्राप्त करने से रोके।